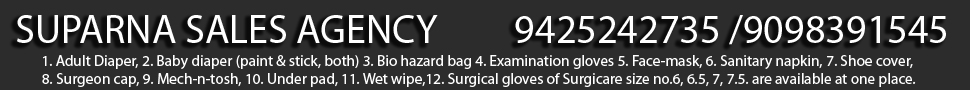शर्म आ रही है उन्हें देख कर ,
जो शर्म बेच खाए हैं।
कल ही की तो बात है,
जो वंदे मातरम नहीं गाए हैं ।
और उन पर भी,
जो बात बात में,
बाँट कर जात पात में ।
संसद के भीतर ,बे कदर
नारे बहुत लगाये हैं ।
शर्म आ रही है उन पर,
जो घटिया मानसिकता से
दूधमुँहे बच्चों से भी ,
प्रतियोगिता के नाम पर ,
भड़कीले नृत्य करवाये हैं।
शर्म आ रही है,
उस फैशन पर,
जिसमें सारा अंग,
झलकता है ।
देवियों के जिस्म से ,
मादकता छलकता है।
किसको किसको कहे यारों,
बूढ़े भी अब बौराये हैं ।
शर्म आ रही है,
उस विकास पर।
जंगलों के ,
महाविनाश पर।
सूखती नदियां, फैलते बंजर ,
दिशाहीन पसरते शहर।
आदरणीयों ने
हरियाली के नाम पर।
सिर्फ दो ठूँठ ही लगाये हैं ।
शर्म आती है उन ,
कलमों पर,
जो पता नहीं,
क्यों मुखरित हो कर।
या हरदम
विष वमन कर ।
गरीबों के आड़ में,
कंगूरों के ही गीत गाए हैं।
शर्म आती है उन्हें देखकर,
जो शर्म बेच खाये हैं।
सप्ताह के कवि

हथबंद, छत्तीसगढ़
 दक्षिण कोसल टुडे
दक्षिण कोसल टुडे