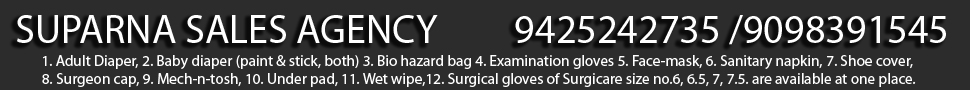किसी ज़माने में राजे -महाराजे भले ही सोने -चाँदी के बर्तनों में भोजन करते रहे हों, लेकिन उस दौर में सामान्य प्रजा के घरों में काँसे और पीतल के बर्तनों का ही प्रचलन था। आधुनिक युग में भी अधिकांश भारतीय घरों में काँसे और पीतल के बर्तनों की खनक लम्बे समय तक सुनाई पड़ती रही, लेकिन पहले एल्युमिनियम और बाद में स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के आने से इनका प्रचलन अब लगभग नहीं के बराबर रह गया है।
फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में शादी -ब्याह में शगुन के रूप में कुछ बर्तन काँसे और पीतल के भी दिए जाते हैं। जैसे -काँसे की थाली, काँसे के लोटे, पीतल की कलशी आदि। लेकिन बावज़ूद इसके, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बर्तनों के बाज़ार में स्टेनलेस स्टील के बर्तनों ने अपनी ज़ोरदार बढ़त बनाकर पुराने जमाने के काँसे और पीतल के बर्तनों के कुटीर उद्योग को एक कोने में ढकेल दिया है।
इसमें दो राय नहीं कि भारत के परम्परागत हस्त शिल्प में काँसा और पीतल के बर्तन कारीगरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता था। हाथों की कारीगरी और कड़ी मेहनत से ये बर्तन तैयार होते थे। आज भी बन रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में। दरअसल कच्चे माल (ताम्बा, जस्ता और रांगा )की बढ़ती कीमतों की वजह से लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है।

छत्तीसगढ़ के पुसौर (जिला -रायगढ़ ) में कभी यह देसी और परम्परागत बर्तन उद्योग अपनी बुलंदियों पर था, जो अब ढलान पर आकर दम तोड़ रहा है। ओड़िशा की सीमा से लगभग लगे और महानदी के नज़दीक बसे पुसौर को वर्ष 2008 में ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बना दिया गया। यह कस्बे नुमा एक बड़े गाँव की तरह है। ओड़िशा की सीमा पर होने के कारण यहाँ ओड़िया भाषा और उत्कल संस्कृति का बहुत गहरा असर महसूस किया जा सकता है। बहरहाल, हम अब यहाँ के डूबते बर्तन उद्योग पर नज़र डालें।
यहाँ बर्तन बनाने का काम कसेर लोग करते थे। इस समुदाय के वरिष्ठ नागरिक वल्लभ कसेर बताते हैं कि बीस -पच्चीस साल पहले पुसौर के लगभग 70 घरों में काँसे और पीतल के बर्तन बनते थे। गलियों में इन धातुओं की खनक गूंजती रहती थी। लेकिन अब केवल चार पांच घरों में ही यह काम होता है, जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। अधिकांश कसेरों ने अपने कच्चे -पक्के, अधपके मकानों में किराना स्टोर या दूसरी तरह की दैनिक जीवनोपयोगी वस्तुओं की दुकानें खोल रखी हैं।
केदारनाथ महाणा 17 वर्ष की उम्र से बर्तन बना रहे हैं। आज वह 65 साल के हैं। उन्होंने और उनके भाई रघुनाथ ने अपने पिता स्वर्गीय दशरथ महाणा से यह काम सीखा था। केदारनाथ का बड़ा बेटा भारतीय सेना में बरेली में पदस्थ है। छोटा लड़का काँसे पीतल के काम को छोड़कर ट्रेक्टर से माल परिवहन का बिजनेस कर रहा है। घर के दो एकड़ की खेती भी संभाल रहा है।

वल्लभ कसेर ने बताया कि बाज़ार में ताम्बा 700 रुपए और रांगा 2000 रुपए किलो मिलता है। जस्ते की कीमत 300 से 500 रुपए या उससे भी कुछ अधिक हो सकती है। नये बर्तन बनवाने के लिए कोई साहूकार (दुकानदार) कच्चा माल लाकर दे तो वे एक दिन में तीन -चार किलो काँसे के नये बर्तन बना सकते हैं। इसके लिए कसेरों को 230 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मज़दूरी मिल जाती है। काँसे के पुराने बर्तनों को गलाकर नया बनवाना हो तो उसके लिए 100 रुपए प्रति किलो की मजदूरी लेते हैं, जबकि पीतल के नये बर्तन बनवाने की मजदूरी 250 रुपए और पुराने को नया बनवाने की मजदूरी 50 से 60 रुपए किलो प्रचलित है। बाज़ार में बर्तन कारोबारी काँसे के नये बर्तन 1400 से 1500 रुपए किलो के भाव से बिकते हैं।
कुछ इसी तरह का अर्थशास्त्र पीतल के बर्तनों का भी है, जिनकी कीमत 900 रुपए से 1100 रुपए के आस -पास है। यानी कारीगर को जितनी मज़दूरी मिलती है, उनके द्वारा निर्मित बर्तन उससे कहीं अधिक रेट पर बाज़ार में बिकते हैं। हालांकि अब इन प्राचीन बर्तनों का बाज़ार सिमटता जा रहा है। वल्लभ कसेर आज से करीब 29 साल पहले अपने तीन -चार नौकरों के साथ बैलगाड़ियों में बर्तन लेकर आस -पास के गाँवों में फेरे लगाकर अपना बिजनेस करते थे। उन्होंने 2012 तक यह काम किया।फिर कड़ी मेहनत के बावज़ूद लागत नहीं निकलने पर उन्होंने यह काम छोड़ दिया।

जीवन बीमा निगम के एजेंट बन गए। उस काम को भी छोड़ दिया। अब खेती करते हैं। उन्होंने मेरी मुलाकात कुछ उन कसेरों से भी करवाई जो आज बर्तनों के इस कुटीर उद्योग को सिर्फ किसी तरह खींच रहे हैं। प्रदीप कसेर, नारायण कसेर और सहदेव कसेर ,ये तीन भाई भी अपने मकान के बरामदे में धौंकनी आदि लेकर बैठे मिले। उनके दो भाइयों में से एक सरकारी नौकरी में है और दूसरा किसी की दुकान में नौकरी कर रहा है। वल्लभ कसेर के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुसौर के अलावा चाम्पा, सक्ति और बाराद्वार भी इन बर्तनों के कुटीर उद्योग का प्रमुख केन्द्र हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ भी पहले जैसी बात नहीं रह गयी है।
काँसे और पीतल के बर्तन बनाने वाले अधिकांश कारीगरों को सारा काम बैठकर और झुककर करना पड़ता है, इसलिए कुछ वर्षों के बाद उनकी कमर और घुटनों में दर्द होने लगता है। बाज़ार में मांग कम, मेहनत ज़्यादा और मज़दूरी भी संतोषप्रद नहीं। ऐसे में स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का मुकाबला कर रहे इस कुटीर उद्योग का दम फूलना और दम तोड़ने की हालत में पहुंचना बहुत स्वाभाविक है।
पुसौर में एक दिलचस्प बात यह देखने को मिली कि बर्तन बनाने वाले अधिकांश कारीगर स्थानीय रामलीला मंडली के कलाकार भी हैं। उनके बारे में फिर कभी। आज तो बस, इतना ही।
आलेख और तस्वीरें :

वरिष्ठ साहित्यकार एवं ब्लॉगर रायपुर, छत्तीसगढ़
 दक्षिण कोसल टुडे
दक्षिण कोसल टुडे