संगीत नामक शब्द से ही मन में स्वर लहरियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, मन और आत्मा दोनो तरंगित हो उठते हैं, देह नृत्य करने लगती है, चेतना अपने उच्चतम स्तर पर उर्ध्वगामी हो जाती है। ऐसा ही है आनंद संगीत और स्वर का। यह एक ऐसी विधा है जिसने मानव को सहस्त्राब्दियों से वश में कर रखा है। कालांतर में लोक और शास्त्र दोनों ही इसमें समाहित हो गए। शास्त्रीय और लोकसंगीत को जानने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि संगीत है क्या? मानव जीवन में संगीत का प्रादुर्भाव हुआ कैसे?
मानव और प्रकृति का अटूट संबंध है। सारी प्रकृति ही संगीत और रसमय है, इसके सानिध्य से ही संगीत की लहरियों का अनुभव हुआ। पक्षियों की चहचहाहट,नदियों व झरनों की कल-कल ध्वनि,पेड़-पौधों के लहराते पत्तों की ध्वनि, घन गर्जना, कोयल की तान, भँवरों का गुंजन, झींगुर, मेंढक, तोता, मैना, पपीहा तथा सागर की ऊँची लहरों के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न लय बद्ध ध्वनि इत्यादि विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनकर मनुष्य को आत्मिक सुख की प्राप्ति हुई और इन आवाज़ से प्रभावित हो कर उसने मुंह से, हाथ की थाप से वैसी ही ध्वनियां निकालने का प्रयास किया। आवाज़ों से हाव-भाव की अभिव्यक्ति हेतु प्रेरित होकर संगीत की सृष्टि की। ध्वनि निकालने एवं उसे हमेशा श्रवण करने के लिए वाद्य यंत्र भी बनाये। इस प्रकार सुवव्यस्थित ध्वनि जो रस या आनंद प्रदान करे, जिसमे स्वर व लय का तालमेल हो संगीत कहलाया।

स्वरुचियों व भावनाओं की अभिव्यक्ति मानव का आदिम स्वभाव है। शैल चित्रों से प्रारंभ हुई अभिव्यक्ति की यात्रा चित्र कला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, काव्य आदि सभी ललित कलाओं के माध्यम से मानव समाज को जोड़ती है, ये एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। संगीत वह ललित कला है जिसमे सुव्यवस्थित ध्वनि जो स्वर व लय के तालमेल से भावाभिव्यक्ति के साथ रस या आनन्द प्रदान करे। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों, मूर्तियों, मुद्राओं, भित्तिचित्रों को देखने से ज्ञात होता है कि हजारों वर्ष पूर्व लोग संगीत से परिचित थे। संगीत का आदिम स्रोत प्राकृतिक ध्वनियां ही रही होंगी। मानव ने उस लय, ध्वनि को परखा भावों में बांधा और संगीत की रचना की जो उसे सुकून देती थी।
प्रागैतिहासिक काल से ही भारत में संगीत की समृद्ध परंपरा रही है। प्राचीन संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी गई है। जिसमे सामवेद प्रमुख है। सामवेद की ऋचाएं गेय ही थीं। संगीत के प्रेरक देव शिव और सरस्वती माने गए। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने नारद को संगीत का वरदान दिया था। सामवेद में मन्त्रों का उच्चारण उस समय के वैदिक सप्तक या समगान के अनुसार सातों स्वरों के प्रयोग से किया जाता था। वेदों में वाद्य यंत्रों का वीणा, कर्करी जैसे तंतु वाद्य, दुंदुभि, गर्गर आदि अवनद्ध वाद्य और घन वाद्य में आघाट, सुषिर वाद्य में तृण, शंख, नाड़ी आदि का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के 30 वें कांड के 19 व 20वें मन्त्र में कई वाद्य यंत्रों के वादन का उल्लेख है।
बिना प्रेरणा के कोई भी कला विकसित नहीं हो सकती, संगीत कला भी उनमें से एक है। संगीत का आध्यात्मिकता से बहुत घनिष्ट संबंध होने के कारण इसे पंचम वेद या गंधर्व वेद कहा गया है वैसे भी सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद को माना गया है। प्राचीनकाल में गुरु शिष्य परंपरा में गुरु द्वारा मौखिक ज्ञान दिया जाता था, जिसे शिष्य कंठस्थ करते थे। श्रुति परम्परा से आने के कारण वेदों व संगीत का कोई लिखित स्वरूप नही होने के पश्चात भी मूल स्वरूप स्थाई रुप से बना हुआ है।।
आचार्य भरतमुनि द्वारा रचित “नाट्य शास्त्र” भारतीय संगीत व इतिहास का लिखित प्रमाण माना जाता है। जिसमे इन्होंने नाटक, नृत्य, संगीत के मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। इसके बाद 12 वीं सदी के पूर्वार्ध में शारंगदेव ने ‘संगीत रत्नाकर’ की रचना की जो सात अध्याय वाला जिसमे संगीत व नृत्य का विस्तार से वर्णन के साथ कई तालों का वर्णन किया गया है। शारंगदेव ने लिखा है “गीतं वाद्यम तथा नृत्यं त्रयम संगीतमुच्यते।” संगीत के स्वरुप को प्रबंध भी कहा जाता था। पहला निबद्ध प्रबंध जो ताल बद्ध गाया जाता था, दूसरा अनिबद्ध जो ताल मुक्त था।

शास्त्रीय संगीत का अपना शास्त्र होता है जिसमे लय बद्धता, गायन, वादन, नर्तन के नियम-उपनियम होते हैं। शास्त्रीय संगीत के स्वरूप, पद्धतियों, शैलियों का वर्णन करने से पूर्व यह जानना महत्वपूर्ण है कि लोक संगीत का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और विद्वानों ने शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोकसंगीत से ही मानी है। संगीत के बिना लोक जीवन प्राणरहित शरीर के समान है।
लोकसंगीत लोक की आत्मा है। लोकगीत प्रकृति के उद्गार हैं जिसमे सामान्य मानव अपनी संवेदनाओं को बड़ी मधुरता और तन्मयता के साथ सहज तरीके से सुर लय और ताल के साथ प्रस्तुत करता है। इन गीतों में उसके सुख-दुःख का वर्णन होता है। लोकगीत व्यक्ति या काल विशेष का ना होकर पुरे समाज का दर्पण होता है। जिसमे मनुष्य अपने आनन्द प्राप्ति हेतु सहज ही अपने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को छंदोबद्ध कर गुनगुना उठता है वहीं से लोकगीतों का स्फुरण होता है।
समाज में प्रचलित विभिन्न संस्कारों, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पक्षों, पर्वों, उत्सवों, ऋतुओं, जीवन में किये जाने वाले विभिन्न क्रिया कलापों को बहुत मार्मिक ढंग से सुर, लय ताल में बांधकर प्रस्तुत किया जाता है। लोकगीत मानवीय संवेदनाओं के हृदय के सहज भाव हैं जो लिखित ना होकर लोक वाणी के रूप में निःसृत होकर आजतक जीवित है। लोक गीतों में धरती, आकाश, पर्वत, नदियां, फसलें गातीं हैं। उन्मुक्त कंठों से जनमानस अपने मन-मस्तिष्क को शांति, ख़ुशी देने हेतु अकेले या समूह में लोक गीत गाते हैं। अर्थात सामान्य जनता के हृदय में बहती स्वछंद और स्वयं उद्भुत भाव धारा जो उन्हें जीवन दर्शन का भी ज्ञान कराती है, वही प्राकृतिक भावधारा ही लोकगीत या लोक संगीत कहलाता है।

हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की चर्चा करते हैं। इसकी दो प्रमुख शैलियां हैं (1) हिंदुस्तानी शैली या उत्तर भारतीय पद्धति।
1.हिंदुस्तानी शैली या उत्तर भारतीय पद्धति :-
ये समूचे उत्तर भारत में प्रचलित है। जिसमे प्रकृति चित्रण, भक्ति व शृंगार की प्रधानता है। मुगलों की छत्र छाया में रहने के कारण इसमें मुस्लिम के साथ-साथ अरबी, फारसी, ईरानी, मध्यएशिया के संगीत का भी प्रभाव पड़ा। हिंदुस्तानी संगीत शैली में लय बनाने के लिए तबला मुख्य वाद्य यंत्र है। तानपुरा की संगति पुरे गायन के दौरान होती है। हारमोनियम और सारंगी की संगत भी रहती है जो फ़ारसी संगीत शैली का प्रभाव है। विभिन्न शैलियों के सम्पर्क में आने के कारण हिंदुस्तानी संगीत पद्धति अपने मूल स्वरूप को बचाये रखने में असमर्थ रही।
इस पद्धति में ध्रुपद सबसे प्राचीन शैली है। इसकी भाषा ब्रज और विषय ईश्वर या राजा के प्रशस्ति गान था। फिर ख़्याल और धमार, ठुमरी, ठप्पा गायन शैली थी। जिसमे ख़्याल शृंगार रस प्रधान, धमार जिसमे कृष्ण संग गोपियों की होली खेलने का वर्णन, ठुमरी भी चंचल शृंगारिक गीत एवं ठप्पा पंजाबी मिश्रित शृंगारिक लच्छेदार गीत है।
2.कर्नाटक संगीत शैली या दक्षिण भारतीय पद्धति:-
दक्षिण के मंदिरों में प्रचलित शैली कलात्मकता से परिपूर्ण भक्ति रस प्रधान होती है। पूजाअर्चना, दार्शनिक चिंतन, नायक-नायिका वर्णन, देशभक्ति आदि विषय इसमे शामिल हैं। पुरंदर दास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। वर्णम, जावाली तथा तिल्लाना प्रमुख शैली हैं। वर्णम में हिंदुस्तानी शैली की ठुमरी की सी समानता है। जावाली भरतनाट्यम के साथ गाया जाने वाला प्रेम गीत और तिल्लाना, तीव्र गीत है, जो उत्तरी भारत के तराना के समान होता है तथ भक्ति प्रधान गीतों की प्रधानता होती है।
दक्षिण कोसल और लोक संगीत व नृत्य करमा
भारतीय संस्कृति अपनी विशाल भौगोलक स्थिति के कारण सबसे अलग है। यहां विभिन्न भाषा, धर्म,खान-पान, विविध क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं, सबकी अपनी संस्कृति, सभ्यता, रीतिरिवाज है परंतु सब मिलजुल कर आपसी सुख-दुःख बांटते है। भारतियों की सहनशीलता, प्रेम,सौहाद्र, सुंदरता, उनकी संस्कृतियों में निहित है। हमारी भारत भूमि एक उद्यान के समान है, जिसमे रंग, सुगंध, आकार, प्रकार के पुष्प रूपी संस्कृतियां हैं जो आपसी एकता की स्वर्णिम आभा पूरे विश्व में बिखेर रही है।
भारत का लोकसंगीत ग्रामीण अंचलों, वनांचलों तथा पर्वतीय अंचलों में बिखरा हुआ है। विविध क्षेत्रों के विविध गीत, नृत्य व वाद्य यंत्र हैं। जिनका कोई लिखित साहित्य तो नही परंतु शैली अवश्य है और इनपर आंचलिकता की विशेष छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है जिसे जानकार ही समझ सकते हैं। शास्त्रीय संगीत के ढांचे में लोकगीत-संगीत नहीं तैयार किये जाते। ये लोक रचित, लोक विषयक और स्वतंत्र गति से प्रवाहित होते हुए गायक और श्रोता को रसानुभूति कराते हैं। लोकगीतों में स्वतंत्रता और उन्मुक्तता होती है जिसे गायक स्वरों के उतार-चढ़ाव को परिवेश विशेष के वाद्य यंत्रों के साथ गाकर तथा स्त्री-पुरुष एकल या सामूहिक रूप से नाचकर भी प्रस्तुत करते हैं।

लोकगीत व नृत्य की बात हो और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति,गीत, नृत्य का उल्लेख न हो तो विषय अधूरा रह जायेगा। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में कला अभिव्यक्ति विविध रूपों में प्रतिष्ठित है, जिसमे लोक जीवन में लोक कलाओं का अप्रतिम योगदान हैं क्योंकि कला का लोकतान्त्रिक स्वरुप लोकाश्रय से ही फलता-फूलता है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व लोकप्रिय पर्व करमा है। इस पर्व पर किया जाने वाला नृत्य व गीत करमा है। जिसकी धुन सुनते ही लोगों के पैर स्वयं थिरकने लगते हैं मन प्रफुल्लित हो उठता है।
सरगुजा अंचल की जन-जातियां मूलरूप से कृषि व वनों पर आश्रित हैं। आदिवसियों को नाच-गाना विरासत में मिला है। मौसम के अनुकूल ही मौसमी राग गए जाते हैं, जो उनके जीवन के हर पहलुओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। मौसमी रागों के कई भेद जैसे फग्गू, खद्दी, टून्टा, जदुरा, धूड़िया, जेठवारी, आसारी, रोपा, अंगनई, करम, अगहनी, बेंजा(शादी) आदि हैं। एक राग के गीतों को भिन्न -भिन्न तरीकों से गाया जाता है।
उरांव परंपरा में रागों का समावेश कुड़ुख और सादरी भाषाओँ में हुआ है। जनजातीय समाज के लोग स्थानीय लोकपर्वों जैसे करमा, छेरता, गंगा दशहरा, हरेली, नवाखाई, तीजा, जीवतिया, देवठन या कार्तिक एकादशी, आठे पर्व या कृष्णजन्माष्टमी इत्यादि में करमा गीत व नृत्य के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते हैं।

करमा गीत के भाव बड़े सुंदर होते हैं। हृदय के सारे भावों को इस गीत में संजोकर बहुत मधुरता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके विषय हास्य रस वाले, पारिवारिक रिश्ते नातों वाले, मज़ाक के, प्यार, तकरार, मान, अभिमान के होतें हैं। करमा शब्द कर्म अर्थात परिश्रम एवं करम अर्थात भाग्य को बताता है। यह पर्व भाद्रपद्र की शुक्ल पक्ष एकादशी को करमी वृक्ष की डाली को आँगन में गाड़कर करम देवता की पूजा-अर्चना एवं व्रत करके मनाया जाता है। तीज पर्व के दिन बांस की टोकरी में जौ, गेहूं, मक्का को बोया जाता है जो करमा तक बढ़ जाता है जिसे जाई कहते हैं। इसमें मिट्टी का दिया जलाकर पूजा कर कथा सुनी जाती है।
करमा गीत में मुख्य वाद्य रूप में मांदर, झांझ, मोहरी या शहनाई का प्रयोग होता है। शास्त्रीय संगीत के प्रमुख वाद्य तबला की थाप व बोल के समान ही मांदर को बजाया जाता है। मांदर के बोल कुछ इस तरह के होते हैं -ताल – “धींग धातुंग तांक तांक”, “धतिंग इतंग तांग, ददंग, तुर्र तुर्र।” महिलाएं गोल घेरा बनाकर नृत्य करती हैं, मध्य में पुरुष गायक, वादक होतें हैं। रोपा के बाद करमा नाच-गान आरंभ होकर तुसगो तक चलता है। करमा के कई भेद जैसे कोट्ठा, मिनसरिया, चाली, रिंजा, रसिका इत्यादि। करमा की तैयारी व स्वागत से लेकर उसे काटकर लाने गाड़ने तथा पूजा-अर्चना कर उसके विसर्जन तक का कार्यक्रम नाचते-गाते ही संपन्न किया जाता है।

करमा पर्व की किंवदंतियां भी है। करम राजा की कहानी एवं करमा व धरमा दो भाइयों की कहानी सुनी सुनाई जाती है। यहां हम कुछ करमा गीतों को देखेंगे जो सुर लय व ताल के साथ मिलकर तन-मन में एक अद्भुत रोमांच एवं उत्साह से भर देता है। करमा गीत के बोल कुछ इस तरह के होते हैं।
करमा गाड़ने के समय गाया जाने वाला गीत–
निकल निकल मझियानी करमा गाडेब
करमा तो आई गेलक रे तोरे अँगने
दे दे मझियानी टीका सिंदुर
किया मा झलक मलक रे
विसर्जन के समय का गीत—
हरे करम केरा, हरे करम केरा
पेलय जोखैंन टुवर नंजा रे
कइले तो आले करम,आइजे तो जाथिस
जा जा करम गंगा किनारे।
करमा गीतों के माध्यम से धरती की सुंदरता, सम्पन्नता उसके गर्भ से मिलने वाले बहुमूल्य संपदा, खनिज पदार्थों का भी बहुत भावपूर्ण वर्णन बड़ी कृतज्ञता के साथ किया जाता है। जो इस गीत में स्पष्ट दिख रहा है-
हैंरे छोटानागपुर! हैंरे हीरा बरवे
नगापुरे जिंगोर-जिंगोर रे
टाटा नू पन्ना, लोहोड़दगा बॉक्साइट,
नगापुरे जिंगोर जिंगोर रे
झरिया नु कुइला, खलारी नू सीमेंट
नगापुरे जिंगोर-जिंगोर
कोडरमा नू अबरक रांची नू बिजली
रांची शहरे जिंगोर-जिंगोर रे
प्रस्तुत गीत में क्षेत्र की विशेषता को बताया गया है। इस प्रकार करमा गीतों में मनुष्य और प्रकृति के अटूट सम्बन्धों को मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लोक कलाकारों के द्वारा लोकगीत-संगीत अपने स्वर,कला, ज्ञान, अनुभव द्वारा ही जीवंत है।
लोक गीत-संगीत का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। जिसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर पाना असंभव है। आधुनिक युग में भी लोगों का इन पारंपरिक गीतों व नृत्य के प्रति उतनी ही रूचि है क्योंकि इनमें जीवन दर्शन एवं मूल्यों की अभिव्यक्ति मुखरित होती है। अतः लोकधर्मी से शास्त्रधर्मी तथा शास्त्रधर्मी से लोकधर्मी की परंपरा सहस्त्रब्दियों से चली आ रही है। इसीलिए हम भारतीय अपनी संस्कृति-सभ्यता के उन्नत स्वरुप को बचाये रख पाने में सफल हुए हैं।
आलेख

हिन्दी व्याख्याता
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़
 दक्षिण कोसल टुडे
दक्षिण कोसल टुडे

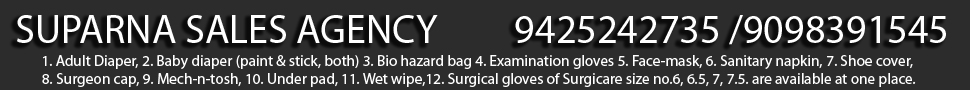

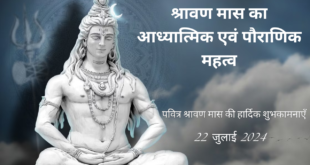

बहुत सुंदर