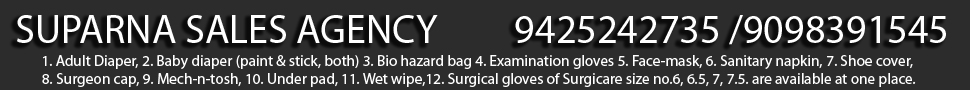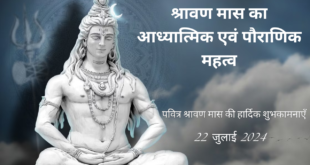लोक संस्कृति का वैभव लोक जीवन के क्रिया-व्यवहार में परिलक्षित होता है। यदि समग्र रूप से समूचे भारतीय लोक जीवन को देखें तो आँचलिकता व स्थानीयता के आधार पर, चाहे व पंजाब हो, या असम हो, कश्मीर हो या केरल, महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल, गुजरात हो या राजस्थान, उत्तरप्रदेश हो या बिहार, उड़ीसा हो छत्तीसगढ़ या अन्य कोई राज्य, सबकी अपनी अलग-अलग लोक संस्कृति है। सबकी लोक संस्कृति का आधार कृषि संस्कृति ही है। कृषि संस्कृति ‘लोक’ का उद्गम है।
छत्तीसगढ़ के लोगो का जीवन कृषि पर ही अवलंबित है। खेती-बाड़ी का कार्य इनकी पूजा है, इनका धर्म है, इनकी प्रकृति है और जहाँ प्रकृति के प्रति लगाव है वहीं जीवन में हरीतिमा है, चाहे यहाँ वन क्षेत्र हो या मैदानी भू-भाग सर्वत्र हरापन है। प्रकति का यह हरापन छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में भी पूरी समग्रता के साथ रूपायित होता है। हरेली, भोजली, जँवारा हो या बसंत पंचमी सभी पर्वों में प्रकृति का मनोरम यप और इसका अप्रतिम सौंदर्य झलकता है। इस रूप-सौंदर्य में जीवन की चारों अवस्थाओं का उल्लास और उत्साह विविध रंगों में बिखरा हुआ है।
छत्तीसगढ़ सदैव श्रम का पुजारी रहा है, चाहे वह किसान हो या अन्य श्रमिक वर्ग। जहाँ श्रम है, वहीं गान है और जहाँ गान है वहीं प्राण है। श्रम का सीधा संबंध उत्सव और पर्वों से है। ये उत्सव और पर्व हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। साथ ही श्रम के पश्चात शरीर की थकान मिटाने के साधन भी। इन साधनों में खेल और मनोरंजन की भी अपनी महत्ता है। श्रम से क्लांत व्यक्ति मनोरंजन के साधन जुटा ही लेता है, व्यक्तिगत तौर पर या फिर सामुदायिक तौर पर। वैयक्तिकता की अपेक्षा सामुदायिकता में सुख और संतोष की अनुभूति अधिक होती है। यूँ तो वर्ष के प्रारंभ का समय लोग अपने-अपने कार्य व्यापार के हिसाब से मानते हैं, किंतु कृषक जीवन में वर्ष का प्रारंभ आषाढ़ माह से माना जाता है। जब आसमान में काली-काली घटाएँ छा जाती हैं। बिजली चमकती है और रिमझिम पानी बरसने लगता है तो सर्वत्र हरियाली छा जाती है। केवल प्रकृति ही हरी नहीं दिखती, बल्कि मनुष्य का जीवन भी हरा होने लगता है। धरती की देह पर कृषक जब अपने हल रूपी कलम से कर्म की गीता लिखता है तब धरती को एक नैसर्गिक सुख की अनुभूति होती है। खेतों में ददरिया की मधुर तान गूंजती है तब ‘हरियाली’ एक ग्रामीण बाला के रूप में थिरकती है। प्रकृति के इस सौंदर्य की आनंदानुभूति सीमेंट-कांक्रीट के जंगल से नहीं, गांव की दहलीज से ही की जा सकती है।

‘हरेली’ हरियाली का लोक रूप है। यह सावन माह में अमावस्या को मनाई जाती है। जब कृषक की बोनी, बियासी पूरी हो जाती है तब वह अपने कृषि औजारों की साफ-सफाई कर उनकी पूजा करता है। नांगर, जुड़ा, रापा, कुदारी, चतवार, हंसिया, टंगिया, बसुला, बिंधना आदि उन सभी औजारों की, जो कृषि कार्य कतई संभव नहीं है। हरेली के दिन प्रातः पशुओं को आटे नमक की लोंदी और वनौषधि खिलाई जा है ताकि वे निरोग रहें। कृषि औजारों की पूजा कर उन्हें ‘चीला और सोहारी’ चढ़ाया जाता है, राऊत गाँव में प्रत्येक घर जाकर घर के मुख्य द्वार पर ‘दशमूर’ और नीम की डंगाली खोंचता है। राऊत का यह कार्य उस घर परिवार के लिए निरोग रहने की कामना का प्रतीक है बदले में गृह स्वामिनी उसे ‘सीधा’ के रूप में चांवल, दाल व द्रव्य देती है। यह लोक मंगल की कामना का अद्भूत उदाहरण है। कुल मिलाकर हरेली कृषि संस्कृति का मंगल पर्व है।
परंतु ‘हरेली’ का यह लोक पर्व इतना भर नहीं है। इसमें बाल जीवन व लोक के क्रीड़ा प्रेम की लंबी अनुगूंज गेड़ी के साथ माह भर सुनाई पड़ती है। हरेली के दिन प्रातः काल से बच्चे गेड़ी के लिए लालयित रहते हैं। बच्चे बाँस लेकर गेड़ी बनाने के लिए बड़े बुजुर्गों से मिन्नत करते हैं। तब उन्हें कहा जाता है पूजा होने दो, तब गेड़ी चढ़ना, पर बच्चे तो बच्चे हैं। वे कब मानने वाले है। स्वतः गेंड़ी बनाने भिड़ जाते हैं। गेड़ी के रों हों चों हों स्वर के साथ गाँव की गलियाँ उनकी किलकारियों और गीतों से गूँज उठती है-
आगे हरेली खपगे गेड़ी
सावन-भादो बाजे रो हों पो पों
सावन भादो…
एक गेड़ी के रो हों पो पों
दू गेड़ी के कोसा काड़ी।
लेजा रे बईमान टूरा
ले जा जी चिन्हारी।।
बाल मन का आनंद और उत्साह देखते ही बनता है। गेड़ी की ऊँचाई सामर्थ्य के अनुसार। किसी की गेड़ी घुटने भर तो किसी की गेड़ी आधा बाँस की, जिसमें चढ़ने के लिए किसी दीवार की सहायता लेनी पड़ती है। ऊँची गेंड़ी वालों को ‘लहोलेत्ता’ भी कहा जाता है। पर बच्चों के लिए ‘लहोलेत्ता’ शब्द भी कम है। गेंड़ी मचने का अपना अलग आनंद है। गेड़ी चढ़ना और मचना सबके वश की बात नहीं। जिन्हें गेड़ी चढ़ने नहीं आता या जो नौसिखिया होते हैं, उन्हें कुशल बच्चे गेड़ी पकड़कर गेड़ी चढ़ना सिखाते हैं। सहयोग और सामूहिकता की अद्भूत मिसाल है गेड़ी। गेड़ी की कोई जात नहीं होती कोई धर्म नहीं होता। गेड़ी-गेड़ी होती है। गेड़ी की पूछती तुम हिन्दू हो या मुसलमान, सिक्ख हो या ईसाई। जिनकी गेड़ी बजती है रो हों पो पों उनके मजे ही मजे। जिनकी गेड़ी नहीं बजती, वे बच्चे गेड़ी में मिट्टी तेल डालकर धूप दिखाते हैं। अब तो गेड़ी को बजना ही बजना है। गेड़ी का यह मोहक शोर मन को विभोर कर देता है। तब बड़े-बूढ़े भी गेड़ी चढ़ने का लोभ संवरण नहीं कर पाते। किसी बच्चे की गेड़ी लेकर अपने स्वर्णिम अतीत को ताजा करते हैं :-
बाँस के डांड़ी बाँस के पउवा
बंधना नरियर बूच के
खुँदा जहू रे लईका हो
रहि हौ दूरिया घूँच के ।।

गेंड़ी का रों हों पो पों सुबह-शाम माह भर गली, गुड़ी, चौरा में सुनाई पड़ता है। कोई रोक न कोई टोक। इस बीच माह भर में गेंड़ी की भेंट अनेक पर्व और त्यौहारों से होती हैं। गेंड़ी की उपस्थिति नागपंचमी, रक्षाबंधन, भोजली, कमरछठ, आठे कन्हैया (श्री कृष्ण जन्माष्टमी), पोरा व तीजा को भी आनंदपूर्ण व प्रभावी बनाती है। बच्चे गेंड़ी को राखी बांधते हैं, भोजली की अगुवाई करते हैं, और कमर छठ के दिन जब माताएँ अपने बच्चों के लिए सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं, तब वही बच्चे गेंड़ी को ‘सगरी’ में डूबा कर नहलाते हैं। कितनी अद्भूत है यह परंपरा लोक के मंगलकामना की पूरी तरह प्रकृति से जुड़ी हुई। परंपरा से बंधी हुई। गेंड़ी का विसर्जन तीजा के दूसरे दिन किया जाता है। तब बच्चे झुंड बनाकर चलते हैं, गेड़ी मचते हैं और विभिन्न मुद्रा में नृत्य भी करते हैं। बस्तर आदि क्षेत्र में तो गेंड़ी नृत्य की परंपरा है। तब बच्चों की गेड़ियों का स्वर गाँव की गलियों से लेकर नदी-कछार व तालाब के पार को भी रोमांचित कर अलोकित आनंद की उत्पत्ति करता है।
आज पोरा काल पोरा।
परन दिन दबी बोरा।
एंसो के गए हरेली
इही दिन के रही अगोरा।।
बच्चे गेंड़ी के पाऊ को नदी-तालाब में विसर्जित कर ‘डाँड़’ घर ले आते हैं। अगले बरस के लिए। शायद यह महंगाई या बाँस की अनुपलब्धता के कारण हो। अब गेंड़ी केवल गाँवों में दिखती है, शहरों में नहीं। शहरी बच्चों के लिए मनोरंजन के तमाम साधन जो आ गए हैं।
‘हरेली’ का पर्व और गेंड़ी मूलतः प्रकृति से सम्पृक्त है। परंतु गेंड़ी की परंपरा कब प्रारंभ हुई इसका उल्लेख नहीं मिलता। पर ऐसी जनश्रुति है कि गेंड़ी की परंपरा पांडवों से जुड़ी हुई है। हमारे शिक्षक थे श्री टी.ए. सिद्धकी। उन्होंने बताया था- महाभारत काल में जब दुष्ट दुर्योधन न पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया तो पांडवों ने आग से बचने के लिए बाँस की गेड़ी बनाकर अपने प्राण बचाए थे। तब से गेड़ी की परंपरा प्रारंभ हुई है। दरअसल लोक, परंपराओं का पोषक होता है। वह इसलिए कि परंपराओं में ही वह अपने जीवन के सुख-दुख, जय-पराजय, हर्ष-विषाद आदि को संजाए रखता है।

यूँ तो छत्तीसगढ़ में विभिन्न पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। सब पर्वों व त्यौहारों को मनाने के लिए भिन्न-भिन्न कारण व परंपराएं हैं। चूंकि ‘हरेली’ से यहाँ पर्वों व त्यौहारों का प्रारंभ होता है। इसलिए इसका अपना विशेष स्थान है। इस दिन दोपहर बाद सारा गॉंव अपनी खुशियों के इजहार के लिए एक मैदान में एकत्र होकर समूहों में विभिन्न खेलों को माध्यम बनाता है। पुरूष वर्ग में चाहे वे बच्चे, बूढ़े या जवान हों या महिला वर्ग में बेटी-बहुएँ या प्रौढ़ महिलाएँ सबके अपने अलग ढंग होते हैं। खुशियों को परस्पर बाँटने व मनोरंजन करने के। कहीं गेंड़ी का शोर है तो कहीं खुडुवा कबड्डी का। कहीं खो-खो तो कहीं फुगड़ी, कहीं बिल्लस, सुर तो कहीं अत्ती-पत्ती, डंडा पचरंगा। गाँव का गौठान हो या स्कूल का मैदान, गाँव के बाहर सड़क हो या चौबट्टा लगता है सारे लोग रंग बिरंगे परिधानों में सजे फूल हैं। जो अपनी परंपरा और उमंग की महक को खुशियों की हवाओं में चारों ओर बिखेरते हैं। बच्चे थकते कहाँ हैं? गौठान में जहाँ बड़ों का खुडुवा (कबड्डी) खेल हो रहा है। वहीं छोटे बच्चे गेंड़ी को रखकर कबड्डी खेलने भिड़ गए बकायदा गीतों के साथ-
खुड़वा के आन तान
खाले बेटा बीरो पान
मैं चलाँव गोटी
तोर दाई पोये रोटी
मैं मारवं मुटका तोर ददा करे कुटका-कुटका…
पकड़ में आ गए तो समझो रोटी जल गई। ‘गड़ी’ मार लिए तो वाह- वाह…
जीत पाल लंका
हनुमान डंका, डंका… डंका… डंका…
अंडा के लकड़ी पटापट टोर
तोर डोकरा मोर पनही चोर… चोर… चोर…
यही विशेषता है छत्तीसगढ़ी खेलों की। खेलों के साथ गीतों की पंक्तियां…
बिच्छी के रेंगना
घर मोर टेंगना -टेंगना-टेंगना…
चल कुत्ता खारे-खार
मोर मेछा लाले लाल…
कोई पकड़ो न यार कोई पकड़ो न यार
चल कबड्डी आवन दे
तबला बजावन दे
तबला में पइसा
लाल पल इचा लाल पलइचा…
खेल जीवन को अनुशासित बनाता है और शरीर को स्फूर्तिवान। खेल की महत्ता तो सर्वविदित है। हरेली के दिन सारा गाँव लोक खेंलों के महाकुंभ में तब्दील हो जाता है। हर उम्र के लोगों के लिए अलग-अलग खेल। बूढ़े-बुजुर्ग जो खेल पाने में असमर्थ होते हैं वे दर्शक बनकर खिलाड़ियों का उत्साववर्धन करते हैं। मित्रवात् प्रतियोगिता, मित्रवत् प्रतिद्वन्दिता आपसी भाई-चारे का अद्भूत नमूना प्रस्तुत करती है हरेली। सभी मगन लोक खेलों की परंपरा में। बच्चों व युवकों की टोली कबड्डी में मगन है तो लड़कियाँ खो-खो में…
अतका बड़ का?
डब्बा
मैं तोर बब्बा।
अतका बड़ का?
बेल
त तोर-मोर हो जाय खेल।
इन पांररिक खेलों के लिए वाहृ साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती।

जहां टोली जुड़ी, इच्छा हुई खेलने की वहीं खेल शुरू हो गया। भला फुगड़ी से कौन अपरिचित होगा? ‘फुगड़ी’ नन्ही लड़कियों का प्रिय खेल है। यह व्यायामपरक खेल है। लड़कियॉं इसे सामूहिक रूप से खेलती हैं। जो अधिक देर तक फुगड़ी खेलती है उसी की जीत मानी जाती हैं। लड़कियाँ उकडू बैठकर तेज गति से दोनों पैर के पंजों को, आगे-पीछे करती हैं। खेल के प्रारंभ में लड़कियाँ सामूहिक रूप से गीत गाती हैं-
गोबर दे बछरू गोबर दे
चारों खूंट ल लीपन दे
चारों देरानी ल बइठन दे
कचरा फेके ले गेयेंव
एक बुंदेला पायेंव
सास बहु खायेंव
देवर ल बिजरायेंव
अपन खाथे गुदा-गुदा
मोला दे् थे बीजा
ओ बीजा ल का करबोन?
रहि जाबो तीजा
तीजा के बिहान दिन
सरी-सरी लुगरा
हेर दे भउजी कपाट के खीला
केंव केंव नरियावैं मंजूर के पीला
एक गोड़ म लाल भाजी
एक गोड़ म कपूर
कतेक ला मानव
मैं देवर-ससुर
आले-आले डलिया
पाके बुंदेलिया
राजा घर के पुतरी
खेल जमुना फुगड़ी
फुन्ना फू फुन्ना फू…
इस फुन्ना फू-फुन्ना फू के साथ फुगड़ी का खेल प्रारंभ होता है।
दरअसल फुगड़ी में स्फूर्ति और संतुलन ही प्रमुख है। जैसे-जैसे लड़कियाँ थकती जाती हैं अपनी हार स्वीकार करती जाती हैं। जीतने वाली लड़की यह पंक्तियाँ गाती हुई फुदकती रहती है-
हारे भउजी हारे रे
लीम तरी पसारे रे
लीम मोर भउजईया
नरियर के बूच
पाछू डर घूंच
तोर डोकरा गाँव गेहे
मोर संग सूत
फुगड़ी गीत में पुरूष प्रधान समाज में नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण है। किस प्रकार यह शोषित और प्रताड़ित होती है। वह समाज में बराबरी की हकदार है। किंतु उसे उसका अधिकार नहीं मिलता।
छोटे हो या बड़े हरेली के दिन सब में नया उत्साह होता है। सबकी अपनी टोली होती है। भला छोटे बच्चे क्यों पीछे रहें। न दौड़ लगाने की जरूरत न उछलकूद करने की जरूरत। बैठे-बैठे ही ‘अटकन-मटकन’ और ‘केऊं-मेऊं मेकरा के जाला’ खेल संपन्न हो जाता है-
अटकन मटकन दही चटाकन
लऊहा लाटा बन में काटा।
सावन में करेला पाकय
तुहुर तुहुर पानी आय
चल-चल बेटी गंगा जाबो
गंगा ले गोदावरी
पाका-पाका बेल खाबो
बेल के डारा टूटगे
भरे कटोरा फूट गे
बिहाती डौकी छूटगे।
ये वे गीत हैं, जो बच्चों को बाल्यावस्था में ही कंठस्थ हो जाते हैं और जिन्हें खेलते समय वे बड़ी तन्मयता के साथ गाते हैं। ये गीत केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि इनमें जीवन-जगत के लिए संदेश भी छिपा है।
लोक खेलों की बात बड़ी निराली हैं। बच्चों की बुद्धि कहाँ-कहाँ तक दौड़ लगाती है। इसका अंदाजा तो बच्चा बनकर ही किया जा सकता है। बालमन की कल्पना का ओर है न छोर। बाल मन बिना पंख के ही अपनी उड़ान पूरी कर लेता है। वैसे भी मन तो बिना डेना की चिड़िया है। बच्चों की टोली में एक बुढिया का अभिनय करता है। उसके हाथ में एक लकड़ी पकड़ा दी जाती हैं, और उस बुढ़िया से अन्य बच्चे प्रश्न करते हैं-
कहाँ जाथस डोकरी?
बुढ़िया उत्तर देती है – मऊहा बीने ल
बच्चे फिर प्रश्न करते हैं – महुं ले लेगबे का ?
बुढ़िया कहती है – तोर दाई ददा ल पूछ के आ।
इस उत्तर के बाद बुढ़िया बने बच्चे को अन्य बच्चे यह कहकर चिढ़ाते हैं-
डोकरी के पीठ में कउँवा चिरकदीस
फिर तो बुढ़िया बना बच्चा चिढ़ाने वाले बच्चों को मारने व दौड़ाने का अभिनय करता है और सारे बच्चे कठल कर हः हः हः हँसते हैं, खुश होते हैं।

वैसे खेलों के लिए किसी दिन या पर्व विशेष की प्रतीक्षा नहीं होती। फिर भी चूंकि हरेली कृषक जीवन का प्रथम त्यौहार है। इसलिए हरेली में विशेष उत्साह होता है। गाँव के सारे लोग इस उत्साह में सहभागी बनते हैं, खेलों में खिलाड़ी या दर्शक के रूप में। अन्य खेलों में बिल्लस, सूर, चर्रा, चूरी लूकौवला, डांडी पऊहा नून बिसऊहा, घोर-घोर रानी इत्ता-इत्ता पानी, घानी मुनी घोर दे, चिंगड़ी बरबट्टी, बितंगी, कांदली, लाठी सुरौला, गिल्ली डंडा, भौंरा-बांटी आदि खेलों को बड़ी सहजता के साथ खेला जाता है। सयाने लोग राम चिंवरा, तिरी चौंक, नव गोठिया आदि में तल्लीन रहते हैं तो किशोर व युवा लोग जोखिम भरे खेल भी खेलते हैं। अत्ती-पत्ती और डंडा पचरंगा ऐसे ही जोखिम भरे खेल हैं। जोखिम इसलिए कि इन दोनों खेलों को पेड़ों पर चढ़कर खेला जाता है। इन खेलो के लिए बरगद का पेड़ उपयुक्त होता है क्योंकि बरगद की डालें और जटाएँ धरती को छूती हैं, जिनके सहारे से ऊपर आसानी सक चढ़ा-उतरा जा सकता है।
‘डंडा पचरंगा’ बड़ा प्राचीन खेल है। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। दुर्योधन भीम को सताता है। खेल में बार-बार भीम से ही दाँव लिया जाता है। इसलिए भीम ने खेल-खेल में वृक्ष को हिलाकर उस पर चढ़े कौरवों को गिरा दिया था-
धाय वृक्ष तब भीम हलाओ
गिरे सबे तो थाह न पायो
पेड़ हलाय दीन्ह जो हाँका
परे भूमि जिमि सब फल पाका।
पंडवानी गायन में भी डंडा पचरंगा का उल्लेख आता है-
डंडा पचरंगा सब खेलन लागे भईया
भीमसेन दामा देवन लागे भाई.
अत्ती-पत्ती में वृक्ष की पत्ती का उपयोग किया जाता है और डंडा पचरंगा में डंडा का। दोनों की प्रक्रिया समान है। अत्ती-पत्ती में दाँव देने वाले से यह कहकर-
अत्ती-पत्ती मार गदत्ती
तुम लाव पीपर के पत्ती।
पत्ती मंगाई जाती है। दाँव लेने वाले चाहे जो पत्ती मंगा सकते हैं। पत्ती मंगाकर वे सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तब दाँव देने वाला लड़का उनकी वांछित पत्ती लाकर पेड़ के नीचे नियत स्थान पर उस पत्ती को दबाकर उन्हें छूने का प्रयास करता है और इधर दाँव लेने वाले नीचे आकर उस पत्ती को छूने का प्रयास करते हैं। इस बीच दाँव लेने वाला कोई उस पत्ती को छू नहीं पाता और दाँव देने वाले लड़के द्वारा उसे छू लिया जाय तो उससे दाँव लिया जाता है। डंडा पचरंगा में पत्ती के स्थान पर डंडा का प्रयोग किया जाता है। इन सारे खेलों में महंगे साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक चीजें ही गांवों में इन खेलों में महंगे साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक चीजें ही गांवों में इन खेलों के साधन बनती हैं।
छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में पर्व और त्यौहारों की बहुलता है। प्रत्येक माह कोई न कोई त्यौहार यहाँ लोक मानस को अपने रंग में रंग लेता है। ये त्यौहार जहॉं लोक जीवन में हंसी-खुशी के अवसर सुलभ कराते हैं, वहीं खेल और मनोरंजन के अनुकूल साबित होते हैं। अन्य त्यौहारों की अपेक्षा ‘हरेली’ की अनुकूलता अधिक है।
शायद ‘हरेली’ का हरापन हमारी परंपराओं में हमारे संस्कारों में और हमारे लोक जीवन में प्राकृतिक हरीतिमा का ज्यादा एहसास कराता है। हरेली का यह हरापन सबके जीवन में बिखरे और निखरे यही कामना है। यह भी कामना है कि भौतिकता की चकाचौंध से परे हमारी खेल परंपराएँ जीवित रहे ताकि माटी से जुड़े ग्रामीण जन शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ रहें। माटी की सोंधी-सोंधी महक हमारे लोक गीतो से आती रहे और खेल परंपरा की यह अविरल धारा निरंतर गतिमान रहे।
आलेख

‘साहित्य कुटीर’ गंडई पंड़रिया जिला राजनांदगांव(छ.ग.) मो. नं. 9424113122
 दक्षिण कोसल टुडे
दक्षिण कोसल टुडे