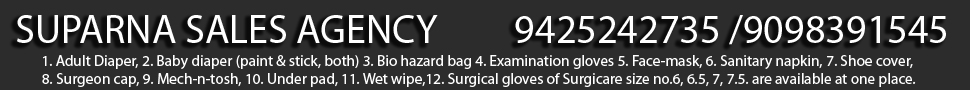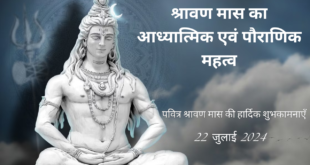मध्ययुगीन भक्ति परम्परा की सिरमौर मीरा बाई उस युग की एकमात्र महिला भक्त संत है जिन्होंने सगुण भक्ति के कृष्णोपासक के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप ही नही छोड़ी वरन उस युग के समाज पर प्रश्न उठाकर समाज की दिशा व दशा निर्धारित करने का बीड़ा भी उठाती हैं।
भक्तिकाल हिंदी साहित्य का ‘स्वर्णिम काल’ कहा जाता है। यही वह काल है जब सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक उत्पीड़न के विरोध में उठा एक सांस्कृतिक आंदोलन उस वेग और गति से उठा कि जिसने व्यक्ति की ऐहिक-ऐंद्रिक सत्ता को झुठला कर परलोक की सम्मोहक अवधारणा समाज के समक्ष रखी।
चाहे हम इस प्यास को उस काल के नैराश्य से उबरने का जिजीविषापूर्ण प्रयास कहें या अपनी क्षीण होती अस्मिता को बचाने की अकुलाहट किंतु यह सत्य है कि भक्ति आंदोलन ने पारलौकिकता के गाढ़े आवरण के बीच व्यक्ति की भौतिक सत्ता, तत्कालीन, समाज-व्यवस्थाऔर संबंधों के महीन अंतर्जाल को गहराई से देखा-परखा और सुधारने का प्रयास भी किया है।
यदि ध्यान से गौर करें तो हम पाते है कि भक्ति काल की रचनाओं में सामाजिक आर्थिक विद्रूपताओं के विरोध में विद्रोही स्वर मुखरित होते है। उस पर भी भक्तिमति मीराबाई एक मात्र ऐसा संत भक्त महिला स्वर है जो सुधारक की अग्निवेदी से उठी एक लपलपाती लपट के रूप में उठ कर अग्निशलाका के रूप में सम्पूर्ण गगन पर आच्छादित हो जाती हैं।
कृष्णभक्त मेड़ता के राव दुदा की पोती, मेवाड़ के वीर शिरोमणि राणा सांगा की पुत्रवधू, वीर भोजराज की पत्नी और राणा विक्रमादित्य की भाभी मीरा में बाल्यकाल से भक्ति के संस्कार पड़े। किंतु मीरा न तो उपर्युक्त सारी उपाधियों उपमाओं से पहचानी जाती है और न ही उनसे तुल्य ही है।
भक्तिमति मीरा बाई वह नाम है जो स्वयं अपने नाम से इन सबको नवीन पहचान देती है और मेवाड़ ही नही सभी भारतीयों को गौरवांवित करती है। एक स्त्री के लिए इतना कर पाना मध्ययुग में ही नही आज भी उतना आसान नही है।पर ‘मीरा’ “मीरा” है निःस्वार्थ पारलौकिक प्रेम में आकंठ डूबी माधुरी रस की अनमोल गीतिका है।
मीरा जो मध्यकाल के सामाजिक वैषम्य में राजवंशों में जन्मी, पली-बढ़ी वह स्वयं उनके सम्पूर्ण काव्य में काल को चुनौती देती मुखर, आक्रामक तेवर लिए प्रकट होती है, वह भी उस युग मे जब एक राजसी कन्या का महल की अटारी पर चढ़ना भी अपराध समझा जाता हो, जब कन्या होना और घर की देहरी लांघना भी असभ्य कहा समझा जाता हो तब कृष्ण प्रेम में आप्लावित मीरा यह कहने का साहस करती है कि–“मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई!”
यह इतना क्रांतिकारी कदम है कि उस युग के तमस में मीरा सुख सुविधाओं में बहती नही, पाखंडों में घिरती नही, राजसी कुल मर्यादाओ का ठीकरा किसी के सिर नही फोड़ती और न ही साधना पथ की ऋद्धियों-सिद्धियों में उलझती है वरन इससे उलट वह एक वेगवती सुरसरि की भांति जिधर से गुजरती है चट्टानी तमस को बिंध कर नवीन तीर्थो का प्रणयन करती चली जाती हैं।
मीरा तमाम सामाजिक बंधनो को लांघ कर हाथ मे इकतारा व मंजीरा लिए गली गली चौखट चौखट कृष्ण प्रेम से गुंजायमान करती है, इतना ही नही वह अपने विरोधियों और सगे सम्बन्धियो से यह भी पूछने का दुस्साहस करती है जैसा कि उनके एक पद में वे कहती है–
“राणाजी थें क्यांने राखों म्हाँसू बैर?
थें तो राणाजी म्हाँने इसड़ा लागो ज्यों ब्रच्छन में कैर!
महल अटारी हम सब त्यागा,त्याग्यो थारो बसनो सहर।
कागज टीकी राणा हम सब त्यागा भगवीं चादर पहर।
मीराँ के प्रभु गिरधरनागर, इमरित कर दियो जहर।।”
अपने दुखों से वह घबराती नही, मार्ग के अवरोधों से वह दिल खोल कर टक्कर लेती है, जूझती है, तथाकथित बुद्धिजीवियों से तर्क-वितर्क करती है और अपना रास्ता स्वयं बनाती है। मध्यकालीन मीरा भक्ति और समाज सुधार की नारी विमर्श की वह मुखर आवाज़ है जो ज्वार की भांति अपने सम्पूर्ण आवेग से न केवल आती है अपितु तमाम नष्ट भ्रष्ट भग्नावशेषों को लील कर अपने वेग में दहाड़ती उफ़ानी लहरों की भांति बहा कर ले जाती है ताकि समाज में नव निर्माण के गीत गुंजायमान हो सकें और तब मीरा व्यक्ति से व्यक्तित्व ही नही एक संपूर्ण कृतित्व हो जाती हैं।
मीरा के सम्पूर्ण चरित और साहित्य का गहराई से अध्य्यन करने पर यह तथ्य उभर कर समक्ष आता है कि मीरा बाई एक युगांतरकारी महिला है जिनके विद्रोही तेवर उनकी सम्पूर्ण रचनाओं में स्पष्टतया व्याप्त है। उनकी सम्पूर्ण भक्ति रचनाएं इस बात की साक्षी है कि मीरा की भक्ति तीन सोपानों से हो कर गुजरती है।
प्रथम सोपान पर जब वह कृष्ण की सगुण उपासना में संलग्न इतनी तल्लीन है कि उसे कोई दूसरा दृष्टव्य ही नही होता। वे कृष्ण की रूप माधुरी मैं रससिक्त प्रज्ञा लिए गा उठती है कि-“माई री ! मैं तो लिया गोविंदा मोल।”,”बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनि मूरति साँवरि सूरति नैणां बने बिसाल। अधर सुधारस मुरली राजति उर बैजंती माल।”,“मैं तो साँवरे के रंग राँची। साजि सिंगार बांधि पग घुँघरूँ लोक लाज तजि नाची।”और “असुवन जल सींचि- सींचि, प्रेम-बेलि बोयी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जा के सिर मोर-मुकट, मेरो पति सोई!”
भक्ति के दूसरे सोपान पर खड़ी मीरा के जीवन मे क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है जब उसके जीवन मे तत्वदर्शी गुरु रैदास का प्रवेश होता है और वह यह जान जाती है कि कृष्ण और राम में तत्त्वतः कोई भेद नही है, जो कृष्ण है वही राम है और तब वह गुरु किरपा को घोषित कर उठती है और गा उठती है कि–“पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु किरपा कर अपनायो!”और “गुरु रैदास मिले मोहे पूरे, धुर से कलम भिड़ी, सतगुरु सैन दई जब आके, जोत से जोत रली!”
साधना पथ के दूसरे पड़ाव पर मीरा गुरु कृपा से भक्ति में अधिक दृढ़ व परिपक्व हो जान जाती है कि सगुण निर्गुण में कोई भेद नही और तीसरे सोपान पर मीरा के पदों में गूढ़ गंभीर रहस्यों को भेदते हुए साधना के रहस्यात्मक अनुभवों का ज्ञान मिलता है और वह पदों में लिखती है कि-“मेरी सूरता प्रभु में रहती मेरी राम नाम धन खेती, सूरत निरत का बैल बनाया ,जब चाहे तब जोती..!” और “सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस बिध होय, गगन मंडल पर सेज पिया की, किस बिध मिलणा होई। ऐ री मैं तो दरद दीवानी मेरो दरद न जाणे कोई!”
इसी सोपान पर वह एक पद में कहती है -“भज मन चरण कँवल अविनासी,कहा भयौ तीरथ ब्रत कीन्हे, कहा लिए करवत कासीं।”और”“त्रिकुटी महल में बना है झरोखा तहाँ तै झाँकी लाऊ री।”तीसरे सोपान पर खड़ी मीरा भक्ति का सार्थक अर्थ जान कर पूर्ण तेजस्विता और पूर्णत्व प्राप्त कर सगुण साकार से निर्गुण निराकार तक की अविरल यात्रा निर्बाध करती नज़र आती है।इसी सोपान पर अपनी भक्ति में पड़ने वाली बाधा को लांघने को उद्यत मीरा तुलसीदास से यह पूछती है कि वह अपने प्रेम-भक्ति मार्ग में बाधक श्वसुर-कुल के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे-
‘श्री तुलसी दुःखहरण, सदा सुखकरण गोसाईं,
बारहु बार प्रणाम करूँ, मोहि देहु बेग समुझाई।
जेते स्वजन हमारे तेते, सबनि उपाधि बढ़ाई,
पूजन-भजन करन नहिं देते, बढ्यो शोक समुदाई।’और जब तुलसीदास उसे परामर्श देते हुए कहते हैं –
“जाके प्रिय न राम, बैदेही,
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही।
तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषण बन्धु, भरत महतारी” तब वह तुरंत निर्णय ले कर मेवाड़ को तज बृज भूमि की ओर प्रयाण करने का निर्णय कर लेती है। उसका इस तरह तत्कालीन संत तुलसीदास जी से विचार विमर्श कर मेवाड़ को त्यागना विस्मित भी करता है और उसकी संकल्प और निर्णय क्षमता का परिचायक हो कर यह भी बताता है कि संतो और बुद्धिजीवियों से तर्क वितर्क व राय विमर्श करने वाली मीरा साधारण प्रकार की नारी नही बल्कि उच्च भूमि पर खड़ी मनस्विनी और चिंतक है जो अपने साधना के हेतु-सेतु गम्भीरता से संकल्पित हो वृंदावन चली जाती है और वहां कभी स्त्री का मुख न देखने की प्रतिज्ञा करने वाले वीतरागी ‘जीव गोस्वामी’ से न केवल शास्त्रार्थ करती है अपितु उस युग मे भी नारी विमर्श के सार्थक प्रश्न पूछ कर उन्हें गूढ़ गम्भीर आध्यात्मिक भेद भी समझाती है।
वह जीव गोस्वामी से यह प्रश्न पूछ कर उनका अज्ञानजन्य पौरुषी दर्प हर लेती है कि-“एक पुरुष सकल जग माही, दूजी नार सोहाई..!”मीरा भक्ति के पूर्णत्व के साथ ज्ञान और प्रेम के संगम पर खड़ी हो जाती है। उनकी सम्पूर्ण रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और प्रेम का अबाध संगम मिलता है। मीरा का भक्ति सागर सरस् अथाह है, जहाँ जब तक चाहो, गोते लगाए जा सकते है। इसमें रहस्य-साधना की गहराई भी समाई है और संतों के सहज योग की ऊंचाई भी मिलती है। मीरा की भक्ति में उद्दामता है, पर अंधत्व नहीं है। उनकी भक्ति-पदों की भावाभिव्यक्ति उनके अनगढ़ भावों के स्पष्ट चित्रण हैं।
मीरा के आरंभिक पदों की कड़ियाँ अश्रुकणों से अत्यंत आद्र हैं। सर्वत्र उनकी विरहाकुलता तीव्र भावाभिव्यंजना के साथ प्रकट हुई है। उनकी कसक प्रेमोन्माद अपने सात्विक रूप में प्रकट होती है। उनका पारलौकिक प्रेमोंउन्माद तल्लीनता और आत्मसमर्पण की स्थिति तक पहुँच गया है।
प्रकृति की पुकार में उनका दर्द और बढ़ जाता है और वह कह उठती है –“मतवारो बादर आयो रे, हरि को संदेसो कबहु न लायै।” परन्तु बाद के पदों में संयोग और सादगी के साथ रहस्यवादी तत्व मुखर हो उठते हैं। उनमें चपलता तो है पर स्थायित्व भी उपलब्ध होता है।
साहित्यिक दृष्टि से उत्कृष्ट मीरा के पदों में श्रृगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्ष पाए जाते हैं, पर उनमें विप्रलंभ शृंगार की प्रधानता है। उन्होंने शांत रस के पद भी रचे हैं। उन्होंने ‘संसार को चहर की बाजी’ कहा है, जो साँझ परे उठ जाती है। मीरा के पदों की भाषा सरल है। उनकी भाषा में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग मिलता है। कहीं-कहीं गुजराती के शब्द भी आ गए हैं।
मीरा के काव्य में कई जगह अपने आप उपमा, रूपक, अतिश्योक्ति, विरोधाभास आदि अलंकार आ गए हैं- ‘दीपक जोऊँ ज्ञान का’, ‘सील संतोस को केसर घोली प्रेम-प्रीत पिचकारी’, ‘विरह-समुंद में छोड़ गया, नेह री नाव चढ़ाव।”,”अगर चंदन की चिता बनाऊ अपने अंग लगा जा जोगी,मत जा मत जा जोगी!” आदि में अलंकारों का सहज प्रयोग दिखाई देता है।
संगीत और कलापक्ष की दृष्टि से मीरा के सभी पदों में उनकी अनुभूति के सहज उच्छ्वास हैं जो गीती काव्य के श्रेष्ठतम उदाहरण कहे जा सकते है। सम्भव है मीरा को यह अनुमान भी न था कि उनके ये उच्छ्वास पदों के रूप में काल के अक्षय भंडार के रूप में संकलित किए जाएँगे क्योंकि वे सायास काव्य नही है भावजनित अनायास झरन की अभिव्यक्ति है उन्हें अलंकारों के आवरण में भावों को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
उनका भावपक्ष इतना सबल है कि कलापक्ष का अभाव उसके नैसर्गिक सौंदर्य को साकार कर देता है। मीरा का काव्य तीव्र भावानुभूति का काव्य है, उसमें भाषा के सजाने-सँवारने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। मीरा के पद गीति-काव्य का चरम उत्कर्ष है। ये पद संगीतज्ञों के कंठहार बने हुए है और आज तक सहृदयों को रससिक्त कर रहे हैं।
गीतिकाव्य में मीरा आज भी अप्रतिम हैं। प्रेमोन्माद, तीव्रता और तन्मयता की त्रिवेणी का पूरा वेग उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। मीरा-काव्य के केंद्र में है मीरा के भीतर की निखालिस स्त्री जो पुरुष-दृष्टि की चौकसी और दबाव से मुक्त हो अपने मनोजगत में दहकती लालसाओं को निर्भीक भाव से व्यक्त कर रही है। वह अपने विरोध की प्रचंडता को भी जानती है, परकीय प्रेम के प्रति दुर्निवार आकर्षण की ‘अनैतिकता’ को भी और अकेले समाज से टकराने के जोखिम को भी।
वर्तमान में स्त्री विमर्श के नाम पर तथाकथित ढिंढोरा पीटने वालो को देखना चाहिए कि मीरा बिना स्त्री विमर्श के नाम पर स्त्री की वह नेतृत्व क्षमता, वह आवाज है जिसे मध्यकाल का संकीर्ण समाज भी दरकिनार नही कर पाया, दबा नही पाया। मीरा स्त्री की आत्माभिव्यक्ति को व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखने की प्रबल संभावना का वह द्वार है जिसे आज की स्त्री विमर्श को नितांत आवश्यकता है। आत्मस्वाभिमान, स्त्रियोचित गरिमा और ओजस्विता का चरम बिंदु जो समाज को एकांतिक पथ पर चल कर भी बदलने का सामर्थ्य रखती है।
मीरा शील की वह संहिता है जो अनलिखी है, धैर्य की वह शीला है जो अगढ़ है किंतु पावन है,पूज्य है। भारतीय समाज व्यवस्था का ढ़ाँचा ही ऐसा है कि अपने रीति रिवाजों और मौखिक संविधान का एक हिंसात्मक पृष्ठ पहले से ही स्त्री के लिए यहां तैयार रहता है। इसकी शुरुआत वर्जनाओं, ताड़नाओ से ही होती है और कभी कन्या के जन्मते ही पर्वतों से नीचे फेंक देने का अभ्यस्त या सती के नाम पर जिन्दा जला देने तक व्याप्त यह जाल हर युग मे किसी न किसी रूप में रहा है।
किसी भी दौर में इन काले विधानों से अकेला लड़ता हुआ व्यक्ति अपने हिस्से में विवशता के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। किंतु भक्तिमति मीरा उससे अकेली पंगा ही नही लेती अपितु अपने दौर में पूरे रूढ़िवादी समाज और कचरा मानसिकता को दो दो हाथ से लड़ कर मात भी देती है और इस लड़ाई को सार्थक मुकाम तक भी ले जाती है।
मीरा का यह संघर्ष भी दोहरा है, क्योंकि वह एक स्त्री है। लोक लाज इस लोक कानून व्यवस्था का एक अध्याय है, मीरा इस पूर्व लिखित संविधान को उस युग मे फाड़कर फैंक देती है और तमाम वर्जनाओं को नकार देती है। ऐसा करने के लिये वह पुरुषों के हिस्से में आरक्षित वीरता को धारण करती है और यह घोषित भी कर देती है कि-“आधे मीरा एकली रे, आधे राणा की फौज” या “तन की आस कबहु नहि कीन्हीं ज्यों रण माहीं सूरौ” या “ग्यान म्हारौ खाँड़े की धार”है।
मीरा के यह पद उस अघोषित युद्ध मे उसकी मर्दानगी के कुछ उदाहरण हैं, वह शंखनाद है जो घटाटोप युद्धोन्माद में घिरे रणकौशल में भी स्त्रियोचित धीरता और वीरता दोनों के अनन्यतम दृष्टांत है। मध्ययुग में भारतीय समाज के दो ही आदर्श थे-‘सती’ और ‘शूरता’।
दोनों दु:खों से लड़ने के लिये दोनों वर्गों के लिये बनाये गये दो अलग अलग हथियार हैं। सती का आदर्श आत्महिंसात्मक है, तो शूर का हिंसात्मक। सती स्त्री जाति की स्वतन्त्रता को आग में जला देने की रणनीति है जो पितृसत्ता ने तैयार की है, तो शूर सामन्तवाद की रक्षा के लिये आत्मोत्सर्ग की नायाब युक्ति है। दु:खों से दोनों ही लड़ते है, अपनी जान देकर और रक्षा होती है दो व्यवस्थाओं की।
अपने स्वयं के लिये उनके पास कुछ भी बचा नही रहता। इनके विरोध में एक ही अवधारणा बचती है और वह है ‘प्रतिहिंसा। किंतु भक्तिमति मीरा बाई सामंती अभिजात्य के इस “प्रतिहिंसा” की अवधारणा को नकारते हुए पूरे सामर्थ्य एव समर्पण से यह युद्ध लड़ती भी है और नारी अस्मिता को बचाते हुए स्वयप्रभा बन कर जग को भी आलोकित करती है।
यह बात अलग है कि कम ही लोग उस काल मे भी मीरा को समझ पाए थे और आज भी उसे आलोचना के नाम पर लांछना देने वालो की कमी नही है। यह सत्य है कि मीरा मध्ययुगीन भक्ति काल का वह चरम सत्य है जो बिना स्त्री विमर्श का नारा लगाए भी समाज को आंदोलित करती है। उन पर गहन पुनर्विचार होना ही चाहिए वरना मीरा के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। मीरा यज्ञवेदी की वह पावन अग्निशलाका है जिससे प्रदूषण मुक्त पर्यावरण निर्मित होता है और जब भी उससे कोई वेदी प्रज्ज्वलित होगी तो रूढ़ियों को समिधा बनना ही होगा।मीरा राजोचित, कुलोचित रहे न रहे रूढ़ियों का हवन जरूरी है।
इसलिए मीरा के साथ न्याय करना ही होगा! मीरा के पदों में जगह जगह उसके साथ होने वाले व्यवहार का रोषपूर्ण वर्णन है किंतु वह सबसे निबटने को संकल्पबद्ध दिखाई देती है। जैसे एक पद में वह कहती है-“लोग कहै मीरा भई बावरी सासु कहै कुलनासी रे, विष का प्याला राणाजी भेज्या पीवत मीरा हाँसी रे, पग घूँघरू बाँध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आपहि हो गई दासी रे।”मीरा की यह उद्घोषणा स्वयं में ही समाज के ठेकेदारों की सबसे बड़ी चुनोती बन जाती है और वे जितना इस आग को बुझाने का प्रयास करते जाते है, वह और भी तेजी से फैलती जाती है।
मीरा की कविता एक अर्थ में स्त्री – मुद्दों की तीखी टीस की कविता है। मीरा का स्त्री-अनुभव इस कविता में तरह तरह से उभर कर आता है। वास्तव में मीरा नारी विमर्श और नारी स्वातंत्र्य की अस्मिता का मध्ययुगीन पूर्ण आंदोलन है जो हर युग मे नाकारा और बेमानी कह कर हाशिए पर धकेल दिया गया है। मीरा को भी उसी आलोचनात्मक रवैये के बारम्बार शिकार होना पड़ता है। किंतु मीरा का प्रश्न न तो उस वक्त के समाज से निरर्थक था, न आज ही खारिज किया जाना चाहिये।
नारी अस्मिताओं को पुनः केंद्र में लाने और उनकी मानवीय गरिमा को पुनर्प्रतिष्ठित करने का पूरा महाभियान ही मीरा है। मीरा की पदावलियों में स्त्री विमर्श अपनी मूल चेतना में स्त्री को पराधीन बनाने वाली पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था का विश्लेषण विवेचन करती है।
मीरा स्त्री को दोयम दर्जे का प्राणी मानने का न केवल विरोध करती है बल्कि स्त्री को एक जीवंत मानवीय इकाई समझने का संस्कार भी देती है। स्त्री-संत हो कर मीरा बहुत कुछ कहती है जिससे यह घिनोना सत्य सामने आता है कि स्त्री का संत होना भी उतना आसान नही है, समाज को स्वीकार नही है क्योंकि उसमें वह निर्बाध बहती है।
पुरुषोचित मानसिकता के ठेकेदारों को मीरा तब भी निंदनीय लगती थी और आज भी प्रश्नचिन्ह ही लगती है क्योंकि उनकी नज़र में स्त्री ऐहिक तो छोड़िए पारलौकिक प्रेम के लिए भी स्वतंत्र नही हो सकती, उन्हें अपनी सत्ता हिलती हुई नजर आती है। किंतु मीरा का सम्पूर्ण व्यक्तित्व-कृतित्व ही विलक्षण है जो चुनोतियों से घबराता नही सामना कर रास्ता बना कर चलता है और भारतीय संस्कारो में रह कर नारी क्रांति को जन्म देता है।
मीरा का उन्मुक्त स्वर में शक्तिसम्पन्न सामंती अभिजात्यों से यह पूछने का दुस्साहस करना ही रूढ़िग्रस्त समाज के मुँह पर पर्याप्त तमाचा है कि-“”राणाजी थें क्यांने राखों म्हाँसू बैर?”मीरा का यह मुखर स्वर नारी का आत्मविश्वास आत्मस्वाभिमानी का उद्घोष भी है और भीतरी स्वयंप्रभा का उज्ज्वल आलोक भी है जिससे पीढ़ियों को मार्गदर्शन मिलता है।
आलेख

 दक्षिण कोसल टुडे
दक्षिण कोसल टुडे