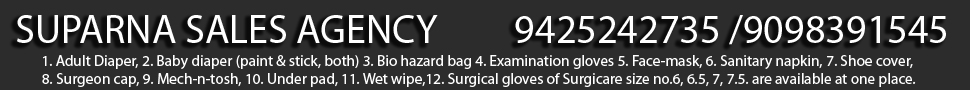एक राष्ट्र के रूप में भारत ने आज तक की अपनी निंरतर ऐतिहासिक यात्रा में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। इतिहास बताता है कि देश के सांस्कृतिक-आध्यात्मिक आधार के कारण किसी एक आध्यात्मिक विभूति की उपस्थिति ने समाज को पतन से उबारा है। तत्कालीन समाज में व्याप्त अज्ञानता, रूढ़ि और कर्मकांड की समाप्ति का कारण था, भारत का अखंड राष्ट्रजीवन। भारत की अखंडता का आधार भूगोल से ज्यादा संस्कृति और इतिहास में है। खंडित भारत में एक सशक्त, एक्यबद्व, तेजोमयी राष्ट्र जीवन खड़ा करके ही अखंड भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ना संभव है।
अविभाजित पंजाब की गुरु परंपरा की इस पुरुत्थान की प्रक्रिया का उज्जवल उदाहरण है। ऐसे समय में जब तुर्क और मुगल मूल के विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचारों से जनता त्रस्त थी और सारे धर्मस्थान भ्रष्ट किये जा रहे थे, तब गुरु नानकदेवजी ने परम आध्यात्मिक सत्य का साक्षात्कार कर अध्यात्म के आलोक में समस्त जनता को सही राह दिखाई। वह बात अलग है कि आज सिख समाज का एक वर्ग अपने हिन्दू मूल से पूर्ण संबंध विच्छेद करने के आवेश में गुरूद्वारों में अरदास से भगवती को हटाने व स्कूलों में से गुरू गोविंद सिंह की रचना “वर दे मोहि शिवा” को हटाने की मांग कर रहा है।
गुरू नानक का जन्म 20 अक्तूबर 1469 राइमोई की तलवंडी नामक गांव में हुआ था। यह गांव वर्तमान लाहौर नगर के दक्षिण पश्चिम, लगभग तीस मील की दूरी पर बसा हुआ है और ननकाना के नाम से प्रसिद्व है। डाक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के शब्दों में “यह भारत के इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण दिन था, जिस दिन संसार में एक महान संदेशवाहक प्रकट हुआ। एक पक्ष से देखा जाए तो गुरू नानक का धर्म भारत की वैदिक परंपरा द्वारा परिचालित सनातन धर्म का ही एक नया आंदोलन था परन्तु गंभीर दृष्टि से देखा जाय तो यह आंदोलन केवल सुधारवादी ही न था इसके अतिरिक्त यह कुछ और भी था।”
आज के हिसाब से यह बात ध्यान देने की है कि नानकदेव जी ने अपनी आध्यात्मिक पूंजी यानी गद्दी अपने बेटों श्रीचंद और लख्मी चंद को नहीं दी। उन्होंने अपने सहयोगी लहना, जिसे उन्होंने अंगद का नाम दिया यानी अंग दा जिसका अर्थ अपना ही अंग मतलब पुत्र, को उत्तराधिकारी बनाया। उन्हीं गुरू अंगद के अमर वाक्य थे, “किरत करो, नाम जपो, वंड चखो।” यानि पुरूषार्थ, प्रार्थना, बांटकर खाना।
नानकदेव सिख धर्म के मूल प्रवर्तक थे। उनके अनन्तर उनके शिष्यों की परंपरा में क्रमशः नव गुरूओं ने उनका प्रचार किया। “आदि ग्रन्थ” में इन सभी गुरूओं तथा बहुत से अन्य संतों की भी रचनाएं संगृहीत है। गुरू नानक देव की बानियां आदि ग्रंथ के अंतर्गत महाला, अर्थात् सर्वप्रथम गुरू के नीचे दी गई पायी जाती है। इनमें शब्द और सलोक अर्थात् साखियां हैं तथा उनके अतिरिक्त, गुरू नानकदेव की रचना जपुजी, असादीवार, रहिरास एवं सोहिला का भी संग्रह है।
तत्कालीन राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए नानकदेवजी ने कलियुग में मूर्ति का सहारा न लेते हुए भी केवल नाम जप के सहारे ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने की बात कही। इस तरह उन्होंने साकार और निराकार दोनों की उपासना को सही मानते हुए कहा-
ऊनराकार आकार आपि निरगुण सरगुण एक।
एक ही एक बखाननो नानक एक अनेक।।
देश काल की परिस्थिति को देखते हुए, जब आये दिन मूर्तियां तोड़ी जा रही हों, नामजप से निराकार की आराधना ही उपयुक्त मार्ग था।
प्रसिद्ध भाषाविद् और साहित्यकार डाक्टर सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि जब इस्लाम ने एक ही रब्ब का दावा करके हिंदू धर्म को चुनौती का प्रतिकार केवल गुरू नानक ने एक निराकार की आराधना पर बल देकर किया। आपने परबह्म को, द्वैत रहित एकमेव निराकार की मान्यता दी। गुरू नानक ने अनेक देवी-देवताओं की पूजा से हटाकर मानवता को एक अकाल की आराधना पर लगाया। इस प्रकार ब्रह्ज्ञान को दर्शाने और दृढ़ निश्चय कराने में आप वैदिक तथा औपनिषदिक ऋषियों के समान थे।
यह बात भी उतनी ही सत्य है कि सिख पंथ निराकार का उपासक है, पर गुरु नानकदेवजी ने साकार की अवहेलना नहीं की है। गुरु नानकदेवजी के शब्दों में ही-
निराकार आकार आपि,
निरगुण सदगुण एक।
एक हि एक बखाननो,
नानक एक अनेक।।
सिख पंथ में दो शब्द है-“गुरुमुख” और “मनमुख”। जो परमात्मा यानी धर्म के पंथ पर चलता है, वह गुरुमुख है। जो अपनी मनमानी करता है, वह मनमुख है। गुरु नानकदेव कहते हैं-विधाता प्रभु ने गुरुमुख के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नाम रूपी पुल बना दिया है। इस नाम रूपी पुल से लंका लूटी गई और काम, क्रोध आदि के दैत्य दुखी हो गए। गुरुमुख रूपी रामचंद्र ने अहंकार रूपी रावण को मारा और विभीषण का भेद को बताना वास्तव में उनका गुरुमुख बनकर ज्ञानवान होना ही है। पत्थर बने जीव भी गुरुमुख बने करोड़ों व्यक्यिों का उद्धार हो चुका है।
नानक देवजी अपने समय में हिन्दू-समाज की अधोगति से पूर्णतरू अवगत थे। यही कारण है कि उन्होंने जात-पांत की व्यवस्था को दरकिनार करते हुए कहा कि एक ज्योति से सब उपजाया-सभी एक ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने सच की वाणी का बखान किया है। सच वाणी ही धर्म है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही इस संपूर्ण ब्रह्माण्ड का आधार है। जब-जब इस आधार पर आघात हुए, इसे कमजोर किया गया, तब-तब मानवता सिमटी सिकुड़ी व मानव समुदाय का अस्तित्व खतरे में पड़ा।
वे इस तथ्य से भी भलीभांति परिचित थे कि सांस्कृतिक पुरुत्थान के लिए जहां एक ब्राह्मण की परिकल्पना को जन-मानस में प्रतिष्ठित करना उपयोगी है, वहां शताब्दियों से चली आती उसकी सगुण-आस्था के मूल स्रोत-पौराणिक युग के देवताओं और उनसे संबंधित कथाओं को सहसा विस्मृत भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए अपने सिद्धांत समर्थन में उन्होंने स्रोतों से उदाहरण चुने-
गौतमु तपा अहिलओ इसत्री, तिसु देख इद्रं लोभाइआ।
सहस सरीर चिह्न भग हूए, ता मनि पछोताइआ।
करउ अठाई धरती भागी, बावन रूप बहाने।।
यह बात कम जानी है कि आदिग्रंथ साहिब में कुछ भाटों की वाणी भी संकलित है, जिससे गुरु-संस्था का यह सांस्कृतिक उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि वह समग्र भारतीय जीवन की चिंतन-धारा से अविच्छिन्न बने रहना चाहते थे। आदिग्रंथ में संकलित भाटों की वाणी का एक अंश इस प्रकार है-
त्रेतै ते माणिक राम रघुवंस कहाइउ।
द्वापरि कृष्ण मुरारि, कंस कितारथ कीउ।
कलजुग प्रमाणु नानक गुरु अंगद अमर कहाइउ।
सचु की वाणी नानक आखे!
सचु की वाणी नानक आखे
सच सुणाइसी सचु की वेला
इतना ही नहीं, श्री गुरुग्रंथ साहिब के राग रामकली में गुरु नानक देवजी के सिद्ध गोष्ठ के अंतर्गत आए एक शब्द में रामसेतु का वर्णन है। जो कि इस प्रकार है-
गुरुमुखि बांधिओ सेतु विधातै।
लंका लूटी दैत संतापे।।
रामचंदि मारिओ अहि रावणु।
भेद बभीखण गुरमुखि परिचायिणु।।
गुरुमुखि सायरि पाहण तारे।
गुरुमुखि कोटि तैतीस उधारे।।
उल्लेखनीय है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 31 राग प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे में लगभग संपूर्ण रचना ही संगीतात्मक है। अगर व्याकरण की बात करें तो अलंकारों में अनुप्रास, उपमा और रूपक स्थान-स्थान पर देखे जा सकते हैं। ऐसे में रूपक और उपमा का उत्कृष्ट उदाहरण गुरु नानक जी की आरती में देखा जा सकता है।
उन्होंने आज के उड़ीसा स्थित पुरी में जगन्नाथजी में हो रही आरती को देखते हुए कहा कि
गगन मै थालु रवि चंदु दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती।।
धूपु मलआनलो पवणु चवरी करे, सगल बनराए फूलंत जोती।।
केवल सगुण ईश्वर ही नहीं गुरु नानकदेवजी ने धरती पर ईश्वर के सगुण प्रतीक यानी मानव मात्र की निस्वार्थ सेवा में पूरा विश्वास जताते हुए उस काम को सर्वोपरि प्राथमिक माना। वे इस कार्य के लिए शीश देकर भी सेवा पाने के इच्छुक थे। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित दोहे इस बात की पुष्टि करते हैं।
तै साहिब की बात जे आखै कह नानक किआ दीजै।।
सीसु बढे करि वैसणु दीजै विणु सिर सेव करीजै।।
जबकि जपुजी के अनुसार,
जिनि सेविआ तिनि पाइआ मानु।।
नानक गाविऐ गुणी निधानु।।
“संत काव्य धारा” पुस्तक में परशुराम चतुर्वेदी गुरु नानकदेवजी के रचना कर्म के विषय में लिखते हैं कि उनकी सर्वप्रसिद्व रचना जपुजी से यह भी प्रकट होता है कि उन्होंने वास्तविक मानवता के पूर्ण विकास के लिए अपना एक विशेष कार्यक्रम भी चला रखा था।
आलेख
राजेन्द्र चड्ढा, जालंधर
 दक्षिण कोसल टुडे
दक्षिण कोसल टुडे