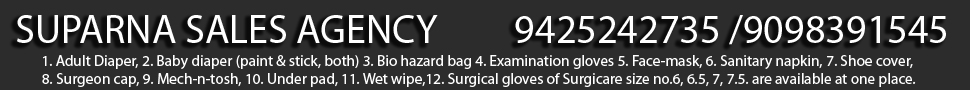छत्तीसगढ़ में धर्म और दर्शन की विविध परम्पराओं और पद्धतियों को प्रश्रय मिला जिसमें शाक्त परम्परा सर्वप्रमुख है जो शैव परम्परा के साथ ही अनुस्यूत है जिसके प्रमाण यहां की मृण्यमयी मूर्तिकला, शिल्प, साहित्य, संस्कृति और जीवन शैली में सहज ही देखे जा सकते हैं।

दक्षिणकोसल में कल्चुरियों से लेकर शरभपुरियों तक तथा फणि नागवंशियों से लेकर छिंदक नागवंशियों तक अपनाए गए शक्ति-उपासना के गूढ़ आयामों को अनुभव किया जा सकता है।

ग्रंथ-भेद से 51 शक्तिपीठों के अंतर्गत दन्तेश्वरी (दन्तेवाड़ा) तथा महामाया (रतनपुर/रत्नावली) की महिमा लोकविश्रुत है। इनके अतिरिक्त डिड़िनेश्वरीदेवी (मल्हार), चन्द्रहासिनी, नाथलदाई (चन्द्रपुर), बिलाईमाता (धमतरी), महिषासुरमर्दिनी (चैतुरगढ़, कोरबा), खल्लारीमाता (महासमुंद), बम्लेश्वरी/बगलामुखी (डोंगरगढ़-कामावतीपुर), कौशल्यामाता (चन्द्रखुरी) आदि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

इनमें से अधिकांश मंदिरों में उलूक व सर्प का अंकन, भैरव आदि की उपस्थिति, बलि-प्रथा का इतिहास, यक्ष-यक्षिणियों की मूर्ति, मिथुन-मूर्तियां शाक्त-तंत्र के प्रतीक हैं। समूचा दक्षिणकोसल शाक्त-परम्परा की रहस्यमयी तंत्र-साधना से भी अविच्छिन्न रूप से जुड़ा है।

शाक्त-तंत्र शास्त्रों में वर्णित मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, आकर्षण, स्तम्भन से लेकर कटोरीचालन, अग्निबाण संचरण, अगिया बेताल, कलवा, चटिया-मटिया, परेतीन, भूतसिद्धी, कचिया-मसान, शव-साधना, शाबर-तंत्र और बहुप्रचारित मूठ के प्रयोग किंवदन्ती के रूप में जनसामान्य में पैठे हुए हैं।

समय-समय पर अनेक भोटियों, बैगाओं और शाक्त-साधकों द्वारा इस सम्बन्ध में अनेक दावे प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। पूरा अंचल टोना, टोटका और टोनही जैसे शब्दों से परिचित हैं। अभिशाप के रूप में बदल चुकी ‘टोनही’ भी अप्रत्यक्षतः प्रतीक में ही सही पर साक्ष्य प्रस्तुत करती है। होली, हरेली, ग्रहण पर घर-घर में किए जाने वाले विविध लोकाचार इसी शाक्त-परम्परा के प्रमाण हैं।
छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव, शहर में थान (देवीचौंरा), लोकमात्रिका (सतबहिनिया-इक्कीस बहिनिया आदि) ठाकुर देवता, भैरव-टीला आदि की उपस्थिति इसी शाक्त-परम्परा की कड़ियां हैं।आवश्यकता है इन विश्रृंखलित परम्पराओं की कड़ियों को उनके दोषरहित स्वरूप में पुनस्र्थापित कर अंचल को उसका खोया वैभव दिया जा सके।
छायाचित्र – ललित शर्मा
आलेख

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
 दक्षिण कोसल टुडे
दक्षिण कोसल टुडे