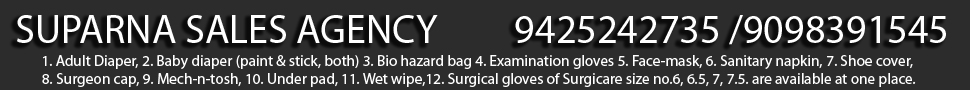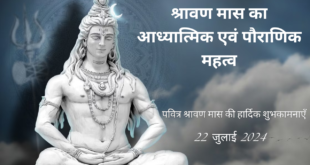“गुरु परम्परा से निरन्तर जो शक्ति प्राप्त होते आयी है, उसी के साथ अपना संयोग स्थापित करना होगा, क्योंकि वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुत्व रहने पर भी गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकेगा। शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु को परामर्शदाता, दार्शनिक, सुहृदय और पथप्रदर्शक के रूप में अंगीकार करें। गुरु करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है।”
- स्वामी विवेकानन्द
स्रोत : भारतीय व्याख्यान, पृष्ठ 426 (व्याख्यान : मैंने क्या सीखा?, ढाका, मार्च 1901)
आषाढ़ माह की पूर्णिमा को सम्पूर्ण भारत वर्ष में ‘गुरु पूर्णिमा उत्सव’ के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन महर्षि वेदव्यास की जयंती होती है। महर्षि व्यास ने भारतीय चिंतन जो कि सृष्टि में व्याप्त परब्रह्म की प्राप्ति की जिज्ञासा की पूर्ति के लिए महान कार्य किया। उन्होंने लक्षावधि वैदिक ऋचाओं को संकलित और सम्पादित किया, इतना ही नहीं तो उसे उचित ढंग से वर्गीकृत भी किया।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ ही भागवत पुराण और श्रीमद्भगवद्गीता को समाज के लिए लिपिबद्ध किया। उन्हीं की कृपा है कि आज हम भाषा, ज्ञान, अनुभव और अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जिस प्रकार की भी सहायता चाहते हैं वह भगवान वेदव्यास द्वारा रचित वेदों और 18 पुराण से प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि वे एक व्यक्ति नहीं वरन् साक्षात् ज्ञान स्वरूप थे। महर्षि वेदव्यास आदिगुरु के रूप में पूजनीय है। इसलिए व्यास पूर्णिमा को ‘गुरु पूर्णिमा’ के रूप में मनाया जाता है।
वैसे तो व्यास अपने आप में एक दायित्व है। शास्त्रों में विद्यमान ज्ञान-दर्शन का अध्ययन कर उसे सामान्य जनता तक इसे सुबोध रूप में प्रचारित करने का कार्य करनेवाले व्यक्ति को भी ‘व्यास’ कहा जाता था। आज भी कथावाचकों को व्यास के रूप में ही जाना जाता है। यही कारण है कि शास्त्रचर्चा के मंच को भी व्यासपीठ कहते हैं। हर वक्ता से व्यासपीठ की गरिमा की रक्षा की अपेक्षा की जाती है।
प्राचीन काल में गुरुकुलों में विद्यारम्भ व स्नातक के रूप में विद्यासमाप्ति के बाद विदाई दोनों इसी दिन हुआ करते थे। इसी दिन ज्ञान पिपासु छात्र अपनी जिज्ञासा व उसके लिए त्याग करने की तत्परता का भाव लेकर गुरु के आश्रम में आते थे। जिसके अन्दर सभी स्तरों पर समर्पण और तप करने की तत्परता हो वही गुरु की छत्रछाया में रहने का अधिकारी होता था। उसी को ‘छात्र’ कहा जाता था।
मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? छात्र जीवन का प्रारम्भ इन्हीं प्रश्नों से होता था, और गुरु अपने अनुभवों, आचरण तथा ज्ञान कौशल के बल से छात्र के सभी प्रश्नों तथा जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। हमारे देश में गुरु-शिष्य परम्परा के अनेक उदाहरण हैं जिनमें महर्षि वशिष्ठ-श्रीराम, महर्षि संदीपनी-श्रीकृष्ण, सदगुरु कबीर साहब-धनि धर्मदास, समर्थ रामदास-शिवाजी महाराज, श्रीरामकृष्ण परमहंस-स्वामी विवेकानन्द आदि।
वेद तथा उपनिषद् में प्रणव मंत्र “ॐ” को प्रथम स्थान पर पूजने की विधि बताई गई है। यह ॐ कार अ, ऊ और म से मिलकर बना है, इसका तात्पर्य है उत्त्पत्ति, संवर्धन और लय। अपने यहां विनाश की संकल्पना नहीं है। क्योंकि कुछ भी समाप्त नहीं होता। हमारी संस्कृति में विसर्जन कहा जाता है अर्थात विशेषत्व से जिसका सृजन होता है। इसलिए ॐ कार विनाश नहीं करता; वह निर्माण, संवर्धन और विसर्जन कर पुनः सृजन करने की शक्ति का स्रोत है।
ॐ कार का उच्चारण करते ही हम वैदिक परम्परा से जुड़ जाते हैं। ॐ कार स्वयं ब्रम्ह का प्रतीक है, इसलिए विवेकानन्द केन्द्र ने ॐ कार को गुरु माना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय इसके संस्थापक आद्य सरसंघचालक डॉ. केशव बलिरामपंत हेडगेवार ने ज्ञान, त्याग व यज्ञ की संस्कृति की विजय पताका परमपूज्य भगवे ध्वज को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। विश्व के सबसे बड़े अनुशासित स्वयंसेवी संगठन के रूप में संघ के विकास का एक प्रमुख कारक यह निर्वैयक्तिक गुरु ही हैं।
प्रतिदिन शाखा में इसी गुरु की छत्रछाया में एकत्रित हो भारतमाता को परमवैभव पर ले जाने की साधना करोड़ों स्वयंसेवक विश्वभर में करते हैं। भारत के सभी सम्प्रदायों और पंथों में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। प्रत्येक समाज में सबसे पहले गुरु की वंदना होती है। पुराणों ने गुरु को सर्वप्रथम पूजनीय बताया है। सदगुरु कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि
“सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोय।
करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय।।”
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु की भूमिका सबसे अधिक होती है। शिष्य अपने गुरु के बताए पथ पर आगे बढ़ता है। शिष्य के जीवन में सदाचार, कौशल, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का विकास गुरु की कृपा से ही संभव होता है। इसलिए शिष्य को गुरु का कृपापात्र होना जरुरी होता है। जिसमें पात्रता नहीं वह कदापि ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। संत कबीर ने शिष्य के पूर्ण समर्पण को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि :-
“पहले दाता शिष्य भया, तन मन अरपे शीश।
दूसर दाता गुरु भया, जिन ज्ञान दिया बख्शीश।।”
शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति कभी भी अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए। गुरु की निंदा व गुरु का विरोध प्रत्यक्ष तो दूर, मन में भी नहीं लाना चाहिए। संत कबीर ने कहा है कि
‘‘गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको नाही मिले भगवाना।”
उन्होंने कहा कि
“कबिरा ते नर अंध है, गुरु को समझे और।
हरि रूठे गुरु शरण हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर।।”
हमारे समाज में गुरु किसे कहा जाए, इसकी अनेक अवधारणा है। हमारे देश में शिशु के जन्मदात्री माता, शिशु की सेवा करनेवाली दाई माँ, नाम रखनेवाले पण्डित, शिक्षा देनेवाले शिक्षक, विवाह सम्पन्न करनेवाले पुरोहित, मंत्र देनेवाला धार्मिक व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार करनेवाला सामाजिक व्यक्ति- ये सभी तो गुरु माने जाते हैं। इन सभी से श्रेष्ठ और महान् गुरु है जो जीव को भय-बन्धन से मुक्त कर दिव्य जीवन प्रदान करता है, इसी गुरु को ‘सद्गुरु’ कहते हैं।
आलेख

 दक्षिण कोसल टुडे
दक्षिण कोसल टुडे